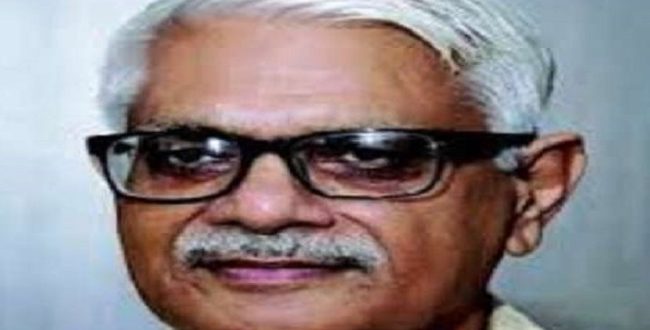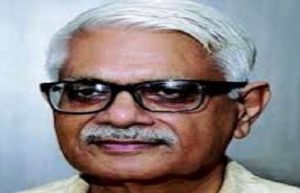
गिरीश्वर मिश्र
राजनीति सामाजिक जीवन की व्यवस्था चलाने की एक जरूरी आवश्यकता है जो स्वभाव से ही व्यक्ति से मुक्त होकर लोक की ओर उन्मुख होती है। दूसरे शब्दों में वह सबके लिए साध्य न होकर उन बिरलों के लिए होती है जो निजी सुख छोड़कर लोक कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में राजनीति में जाना सुख की लालसा से नहीं बल्कि अनिश्चय और जोखिम के साथ देश की सेवा की राह चुनना था। स्वतंत्रता मिलने के बाद धीरे-धीरे राजनीति की पुरानी स्मृति धुंधली पड़ने लगी और नए अर्थ खुलने लगे। जिसमें देश, लोक और समाज हाशिए पर जाने लगे और अपना निजी हित प्रमुख होने लगा। यह प्रवृत्ति हर अगले चुनाव में बलवती होती गई और अब सत्ता, अधिकार और अपने लिए धन-संपत्ति का अम्बार लगाना ही राजनीति का प्रयोजन होने लगा है।
राजनैतिक विचारधारा और आदर्श अब पुरानी या दकियानूसी बात हो चली है। विचार स्वातंत्र्य इतना कि अब मुद्दों पर सहमति हो जाय तो कोई भी दल किसी भी दल यहाँ तक कि अपने धुर विरोधी दल के साथ भी सरकार बना लेने को आतुर रहता है। नेताओं के चित्त इतने उदात्त कि उनके लिए केंद्र में साथ और राज्य में विरोध भी सहजता से ग्राह्य हो जाता है। इसी तरह लगभग हर राजनैतिक दल अपनी कार्यप्रणाली में लोकतांत्रिक तौर-तरीकों को पीछे छोड़ता जा रहा है। मसलन अब सुप्रीमो और हाईकमान ही हर काम के लिए अधिकृत होने लगा है। दल के कार्यकर्ताओं की भूमिका भी जमीन से नहीं ऊपर से तय होने लगी है। सत्ता की बन्दरबाँट और सौदेबाजी हर स्तर दिखने लगी है। दिक्कत होती है तो एक छोटे राज्य में कई-कई उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। इस तरह सत्ता के समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए हरसंभव युक्ति अपनाया जाना स्वीकार्य हो चुका है।
सिद्धांत में लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता ही प्रमुख होती है। फलत: राजनीति जन जीवन में उपजती है और वहीं से जीवन ग्रहण करती है। परन्तु भारतीय जन जीवन में राजनीति पर राजनेताओं का एकाधिकार होता जा रहा है। राजनेता अपने आचरण में लोक से दूर होते जा रहे हैं और नए नेताओं के बीच सेवा और त्याग जैसे विचार अपनी चमक खो रहे हैं। अब राजनीति करना महँगा सौदा बन चुका है और किसी साधारण आदमी के बस से बाहर हो चुका है। मजबूरी में राजनीति सौदेबाजी पर टिक जाती है और जो लोग धन देते हैं उसकी कीमत भी वसूलते हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की जो सीमा तय की है वह अवास्तविक है। ऐसे में राजनीति का प्रवेश द्वार उन चुनिंदा लोगों के लिए होता है जो खर्च में समर्थ होते हैं। इस तरह नैतिकता और जनसेवा आदि के मूल्य पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। भारतीय राजनीति की इस बदलती संस्कृति में उदारता है और उसमें किसी का भी प्रवेश हो सकता है। जो लोग प्रवेश पा लेते हैं वे पूरी व्यवस्था को अपने लायक बना डालते हैं और अपने सरीखे लोगों को अधिकाधिक प्रश्रय देते हैं। यह अद्भुत विसंगति है कि जहां राजनीति देश के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है वहीं राजनीतिज्ञ होने लिए किसी तरह की योग्यता अनिवार्य नहीं है। समावेशी होने के लिए इस तरह के बंधन अमान्य हो जाते हैं और कोई भी जीत कर सिकंदर बन सकता है।
जिन लोगों में राजनीति के प्रति आकर्षण और रुझान दिख रही है वे सत्ता और अधिकार के भूखे हैं। विभिन्न पार्टियों के दफ्तर में चुनाव में प्रत्याशी होने के लिए टिकटार्थियों की भीड़ देखने से इसका अंदाजा लगता है। अंतत: जिनको पार्टी टिकट देती है वे होते हैं जिनकी योग्यता से अधिक जीतने की संभावना होती है। यहाँ जाति, धन और असर के बाद योग्यता का नंबर आता है। शिक्षा संवैधानिक पद के कार्यभार को संभालने के लिए जरूरी है इससे सहमति के बावजूद मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति पद तक के लिए व्यवस्था ने समझौते किए हैं। व्यवहार के स्तर पर देखें तो यह बात साफ़ जाहिर हो रही है कि राजनीति में आकर मंत्री पद को संभालने के लिए अब किसी तरह के ज्ञान और कौशल की जरूरत नहीं रह गई है और कोई भी नेता किसी भी मंत्रालय को संभाल सकता है। जबकि परिस्थतियों की जटिलता ज्ञान के अधिकाधिक वैशिष्ट्य की ओर संकेत करती है।
आज राजनीति में शामिल लोगों की आम आदमी के मन में जो छवि बनती जा रही है उसमें अपराध, अनधिकार चेष्टा, बल प्रयोग और अपने लाभ के अवसर बढ़ाना आदि प्रमुख होते जा रहे हैं। उनके लिये जनता का अर्थ अपने परिजन, अपनी जाति-बिरादरी और अपने क्षेत्र तक सीमित होता जा रहा है। स्थिति यह है अब नेता लोगों को देश-दुनिया के बारे में भी जानकारी नहीं होती और सार्वजनिक स्थलों पर हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। राजनीतिज्ञ के लिये सुशिक्षित होना जरूरी नहीं होने से महत्वाकांक्षा ही एकमात्र आधार बचा है। राजनीति और शिक्षा का सम्बन्ध टूटता जा रहा है क्योंकि राजनीति में सफलता के सूत्र सेवा, ज्ञान और कौशल की जगह धनबल, जनबल और बाहुबल होते जा रहे हैं।
वंशवाद की बेल जिस तरह तेजी से विभिन्न दलों पर काबिज हो रही है उससे राजनीति को निजी सत्ता में तब्दील करने की प्रवृत्ति को बल मिल रहा है। नेतागण अपने को जनता के बीच कम सहज पाते हैं। सुरक्षित रहने और अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए परिवार के बीच सत्ता को अधिकार में रखने को उद्यत रहते हैं।
यह निरा संयोग नहीं कहा जा सकता कि जेल में रहकर भी कई बाहुबली चुनाव में विजयी हो जाते हैं और शुद्ध अपराधी चरित्र के लोग राजनैतिक शक्ति हासिल कर लेते हैं। राजनीति की इस तरह की मजबूरियां अंतत: निहित स्वार्थ की ही पूर्ति करती नजर आती हैं। राजनीति के द्वार ऐसे जनों के लिये ही खुलते हैं। ताजा चुनाव में हर दल में ऐसे उम्मीदवार अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में हैं जिनकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की प्रवृति रही है। चुनावी समर में उनके व्यवहार और बातचीत से भी इसका सहज अनुमान लगाया जाता है कि समाज के हित के लिए उनकी संलग्नता कितनी सतही है। प्रत्याशी लोग झूठ-सच कुछ भी बोल कर मतदाताओं को रिझाते हैं। इस दौर में शराब और रुपये की वैध-अवैध खपत और पुलिस की पकड़-धकड़ के किस्से भी सुनाई पड़ते हैं। मानों वोट न हो कोई जिन्स हो बाजार में जिसकी खरीद-फरोख्त हो रही हो। आरोप-प्रत्यारोप, दावे और वादे के साथ धनबल, जातिबल और बाहुबल की सहायता से सत्ता पर काबिज होने की हरसंभव जुगत की जाती है। ऐसा करते हुए चुनाव प्रचार संघर्ष में भी बदल जाता है और अपराध की हद में चला जाता है।
आए दिन ये राजनैतिक करतब यहां-वहां दुहराए जाने लगे हैं। देश-दुनिया और समाज की समस्याओं और नीतियों पर चर्चा छोड़ जनसभाएं वोट की बोली लगाने जैसे माहौल में आयोजित होने लगी हैं। यह राजनैतिक सरगर्मी जिसमें नेताजी अपने इलाके की सुधि ले पाते हैं अल्पकालिक ही होती है क्योंकि जीतने या हारने के बाद नेताजी प्राय: लुप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर चुनावी और गैर चुनावी राजनैतिक आचरण लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से असंतोषजनक होती जा रही है। यह खेद की बात है कि छोटे बड़े-नेता अल्पकालिक निजी लाभ के सामने देश के नुकसान की अनदेखी करने में कोई संकोच नहीं करते। लोकतंत्र को चलाने के लिए लोकतांत्रिक जीवनशैली भी जरूरी है इसलिए राजनैतिक दलों की संस्कृति में लोकतंत्र के संस्कार स्थापित करने आवश्यक हैं।
(लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विवि, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)
 Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।